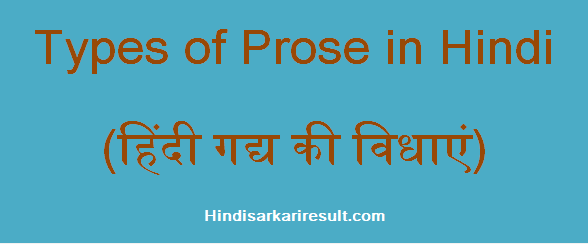Hindi Gadya ki Vidhaye/ Types of Hindi prose
हिंदी गद्य की विधाओं को दो भागों में बांटा गया है:
- प्रमुख विधाएं
- गौण या प्रकीर्ण विधाएँ
इसमें से पहला वर्ग प्रमुख विधाओं का है जिसमें नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध, और आलोचना को रखा जा सकता है। दूसरा वर्ग गौण या प्रकीर्ण गद्य विधाओं का है। इसके अंतर्गत जीवनी, आत्मकथा, यात्रावृत, गद्य काव्य, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्ताज, डायरी, भेंटवार्ता, पत्र साहित्य, आदि का उल्लेख किया जा सकता है।
प्रमुख विधाओं में नाटक, उपन्यास, कहानी, तथा निबंध और आलोचना का आरंभ तो भारतेंदु युग सन (1870 से 1900) में ही हो गया था किन्तु गौण या प्रकीर्ण गद्य विधाओं में कुछ का विकास द्विवेदी युग और शेष का छायावाद तथा छायावादोत्तर युग में हुआ है।
द्विवेदी युग में जीवनी, यात्रावृत, संस्मरण, पत्र साहित्य आदि का आरंभ हो गया था। छायावाद युग में गद्यकाव्य, संस्मरण और रेखाचित्र की विधाएं विशेष रूप से समृद्ध हुई। छायावादोत्तर युग में प्रकीर्ण गद्य विधाओं का पूर्ण विकास हुआ। आत्मकथा रिपोर्ताज, भेंटवार्ता, व्यंग्य, विद्रूप लेखन, डायरी, एकालाप, आदि अनेक विधाएं इस युग में विकसित और समृद्ध हुई। Hindi Gadya ki Vidhaye
यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि प्रमुख गद्य विधाएं अपनी रूप रचना में एक दूसरे से सर्वथा स्वतंत्र हैं जबकि प्रकीर्ण गद्य विधाओं में से अनेक, निबंध विधा से पारिवारिक संबंध रखती हैं। एक ही परिवार से संबंध रखने के कारण यह एक दूसरे के पर्याप्त निकट प्रतीत होती हैं।
हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं
नाटक
नाटक रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई एक रचना होती है जिसमें पात्रों एवं संवादों पर आधारित एक या एक से अधिक अंक होते हैं। नाटक वस्तुतः रूपक का एक भेद है। रूप का आरोप होने के कारण नाटक को रूपक भी कहा जाता है। अभिनय के समय नायक पर किसी ऐतिहासिक चरित्र जैसे दुष्यंत, कृष्ण, राम, आदि पात्र का आरोप किया जाता है, इसीलिए इसे रूपक कहते हैं। नट (अभिनेता) से सम्बद्ध होने के कारण इसे नाटक कहते हैं। नाटक में ऐतिहासिक पात्र विशेष की शारीरिक व मानसिक अवस्था का अनुकरण किया जाता है। नाटक शब्द अंग्रेजी शब्द ड्रामा या प्ले का पर्याय बन गया है। हिंदी में मौलिक नाटकों का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। द्विवेदी युग में इसका अधिक विकास नहीं हुआ। छायावाद युग में जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक नाटकों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। छायावादोत्तर युग में लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्रनाथ अश्क, सेठ गोविंद दास, डॉ. रामकुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, आदि ने इस विधा को विकसित किया है। Hindi Gadya ki Vidhaye
इसे भी पढ़ें: गद्य की परिभाषा और उदहारण
नाटकों का एक महत्वपूर्ण रूप एकांकी है। एकांकी किसी एक महत्वपूर्ण घटना, परिस्थिति या समस्या को आधार बनाकर लिखा जाता है और उसकी समाप्ति या पटाक्षेप एक ही अंक में कर दिया जाता है। हिंदी में एकांकी नाटकों का विकास छायावाद युग से माना जाता है। सामान्यत: श्रेष्ठ नाटककारों ने ही श्रेष्ठ एकांकीओं की भी रचना की है।
उपन्यास
हिंदी में उपन्यास शब्द का आविर्भाव संस्कृत के उपन्यस्त शब्द से हुआ है। उपन्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ है सामने रखना। उपन्यास में प्रसादन अर्थात प्रसन्न करने का भाव भी निहित है। किसी घटना को इस प्रकार लिखकर सामने रखना कि उससे दूसरों को प्रसन्नता हो, उपन्यास कहलाता है। किंतु इस अर्थ में उपन्यास का प्रयोग आजकल नहीं होता। हिंदी में उपन्यास शब्द अंग्रेजी नावेल का पर्याय बन गया है। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित परीक्षा गुरु को माना जाता है। मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास को सामाजिक-सामयिक जीवन से सम्बद्ध करके एक नया मोड़ दिया था। वे उपन्यास को मानव चरित्र का चित्रण समझते थे। उनकी नजर में मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। वस्तुतः उपन्यास हिंदी गद्य साहित्य का वह महत्वपूर्ण कलात्मक विधा है जो मनुष्य को उसकी समग्रता में व्यक्त करने में समर्थ है। प्रेमचंद के बाद जैनेंद्र, इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय, यशपाल, उपेंद्र नाथ अश्क, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, नरेश मेहता, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती, राजेंद्र यादव, आदि लेखको ने हिंदी उपन्यास साहित्य को समृद्ध किया है।
कहानी
जीवन के किसी मार्मिक तथ्य को नाटकीय प्रभाव के साथ व्यक्त करने वाली, अपने में पूर्ण कलात्मक गद्य विधा को कहानी कहा जाता है। हिंदी में मौलिक कहानियों का आरंभ सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के बाद हुआ। कहानी या आख्यायिका हमारे देश के लिए नई चीज नहीं है। हमारे पुराणों में भी शिक्षा, नीति एवं हास्य-प्रधान अनेक कहानियां उपलब्ध हैं किंतु आधुनिक साहित्य कहानियों का उद्देश्य और शिल्प उनसे भिन्न है। आधुनिक कहानी जीवन के किसी मार्मिक तथ्य को नाटकीय प्रभाव के साथ व्यक्त करने वाली अपने में पूर्ण एक कलात्मक गद्य विधा है, जो पाठक को अपनी यथार्थपरता और मनोवैज्ञानिकता के कारण निश्चित रूप से प्रभावित करती है। हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रेमचंदोत्तर या छायावादोत्तर युग में जैनेंद्र, अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी, यशपाल, उपेंद्र नाथ अश्क, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, अमरकांत, मोहन राकेश, फणीश्वर नाथ रेणु, बृजेंद्र नाथ निर्गुण, शिवप्रसाद सिंह, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी, शिवानी, निर्मल वर्मा, आदि लेखकों ने इस दिशा को अधिक कलात्मक तथा समृद्ध बनाया है।
आलोचना
आलोचना का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु को भली प्रकार देखना। जिस प्रकार किसी वस्तु को भली प्रकार देखने से उसके गुण दोष प्रकट होते हैं, ठीक उसी तरह किसी साहित्यिक रचना को भली प्रकार देखकर उसके गुण दोषों को प्रकट करना ही उसकी आलोचना करना कहलाता है. आलोचना के लिए समीक्षा शब्द का भी प्रचलन है। इसका भी लगभग यही अर्थ है। हिंदी में आलोचना अंग्रेजी में क्रिटिसिज्म शब्द का पर्याय बन गया है। हिंदी में आधुनिक पद्धति की आलोचना का आरंभ भारतेंदु युग के बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी ‘प्रेमघन’ द्वारा लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर नाटक की आलोचना से माना जाता है। आगे चलकर द्विवेदी युग में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, बाबू श्यामसुंदर दास, लाला भगवानदीन, आदि ने इस क्षेत्र में विशेष कार्य किया। हिंदी आलोचना का उत्कर्ष आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना कृतियों के प्रकाशन से मान्य है। आचार्य शुक्ल के बाद बाबू गुलाब राय, पंडित नंददुलारे वाजपेई, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉ नागेंद्र, डॉ रामविलास शर्मा, की हिंदी आलोचना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। Hindi Gadya ki Vidhaye